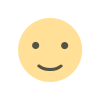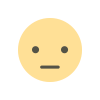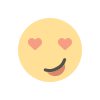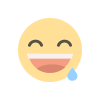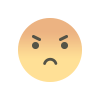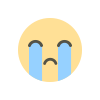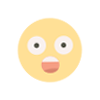बेरोज़गारी और युवा रोज़गार: वैश्विक संकट का समाधान
बेरोज़गारी, खास तौर पर युवाओं के बीच, एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती है जिसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हैं। यह लेख बेरोज़गारी और युवा रोज़गार की जटिल गतिशीलता का पता लगाता है, इसके कारणों, परिणामों और संभावित समाधानों का विश्लेषण करता है। शिक्षा, आर्थिक नीति, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण की भूमिकाओं की जांच करके, यह लेख युवा रोज़गार संकट का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और दुनिया भर में युवाओं के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ रोज़गार के अवसर बनाने की रणनीतियों पर प्रकाश डालता है।

INDC Network : जानकारी : सामाजिक मुद्दे : बेरोजगारी और युवा रोजगार: वैश्विक संकट का समाधान
परिचय : बेरोजगारी हमारे समय की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जो विभिन्न आयु समूहों, क्षेत्रों और क्षेत्रों के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बेरोजगारी के सबसे अधिक शिकार युवा लोग हैं, जिन्हें अक्सर श्रम बाजार में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। युवा रोजगार संकट एक जटिल मुद्दा है जिसके गहरे कारण हैं, जिनमें अपर्याप्त शिक्षा और कौशल बेमेल से लेकर आर्थिक अस्थिरता और तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति शामिल है। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित होती जा रही है, युवाओं के लिए सार्थक और टिकाऊ रोजगार के अवसर प्रदान करने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है।

इस लेख का उद्देश्य बेरोज़गारी और युवा रोज़गार का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे के कारणों, परिणामों और संभावित समाधानों की खोज करना है। शिक्षा, आर्थिक नीति, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के बीच परस्पर क्रिया की जांच करके, लेख युवा बेरोज़गारी को बढ़ावा देने वाले कारकों पर प्रकाश डालने और वैश्विक रोज़गार संकट से निपटने के लिए रणनीतियाँ पेश करने का प्रयास करता है।
बेरोज़गारी और युवा रोज़गार को समझना
बेरोजगारी और युवा रोजगार की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए इन अवधारणाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझना आवश्यक है।
बेरोज़गारी की परिभाषा: बेरोज़गारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें काम करने में सक्षम और सक्रिय रूप से काम की तलाश करने वाले व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। बेरोज़गारी दर आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है और इसकी गणना उस श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में की जाती है जो बेरोज़गार है और सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रही है।
बेरोज़गारी के कई प्रकार हैं:
-
घर्षणात्मक बेरोज़गारी : यह तब होता है जब व्यक्ति नौकरी बदलने या पहली बार श्रम बाज़ार में प्रवेश करने के दौरान अस्थायी रूप से बेरोज़गार हो जाता है। यह अक्सर अल्पकालिक होता है और इसे गतिशील श्रम बाज़ार का एक सामान्य हिस्सा माना जाता है।
-
संरचनात्मक बेरोजगारी : इस प्रकार की बेरोजगारी तब पैदा होती है जब कार्यबल के कौशल और नियोक्ताओं की जरूरतों के बीच कोई बेमेल होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी अक्सर दीर्घकालिक होती है और प्रौद्योगिकी में बदलाव, उद्योग में गिरावट या उपभोक्ता मांग में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती है।
-
चक्रीय बेरोजगारी : चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक चक्र से संबंधित है। आर्थिक मंदी या मंदी के दौर में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है, जिससे नौकरियां चली जाती हैं। इसके विपरीत, आर्थिक विकास के दौर में मांग बढ़ जाती है और बेरोजगारी दर में गिरावट आती है।
-
मौसमी बेरोज़गारी : इस प्रकार की बेरोज़गारी मौसमी प्रकृति के उद्योगों में होती है, जैसे कृषि, पर्यटन और निर्माण। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को ऑफ-सीज़न के दौरान बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है।
युवा रोजगार और बेरोजगारी: युवा रोजगार का तात्पर्य श्रम बाजार में युवा लोगों (आमतौर पर 15 से 24 वर्ष की आयु) की भागीदारी से है। दूसरी ओर, युवा बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है, जहां काम करने के इच्छुक और सक्षम युवा लोग नौकरी पाने में असमर्थ होते हैं। अनुभव की कमी, कौशल बेमेल और श्रम बाजार में प्रवेश में बाधाओं सहित कई कारकों के कारण युवा बेरोजगारी अक्सर समग्र बेरोजगारी दर से अधिक होती है।
युवाओं के लिए रोजगार कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
-
आर्थिक विकास : युवा रोजगार उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में योगदान देता है।
-
सामाजिक स्थिरता : रोज़गार युवाओं को उद्देश्य, पहचान और सामाजिक समावेश की भावना प्रदान करता है। युवा बेरोज़गारी के उच्च स्तर से सामाजिक अशांति, अपराध और राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है।
-
व्यक्तिगत विकास : रोजगार युवाओं को आवश्यक कौशल विकसित करने, कार्य अनुभव प्राप्त करने और नेटवर्क बनाने में मदद करता है जो दीर्घकालिक कैरियर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
युवा बेरोज़गारी का वैश्विक परिदृश्य
युवा बेरोज़गारी एक वैश्विक मुद्दा है जो विकसित और विकासशील दोनों देशों को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, 2021 में वैश्विक युवा बेरोज़गारी दर 14.6% थी, जो समग्र बेरोज़गारी दर से दोगुनी से भी ज़्यादा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका जैसे कुछ क्षेत्रों में, युवा बेरोज़गारी दर 25% से ज़्यादा है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ पेश करती है।
क्षेत्रीय भिन्नताएं: युवा बेरोजगारी दर विभिन्न क्षेत्रों और देशों में काफी भिन्न होती है, जो आर्थिक स्थितियों, श्रम बाजार की गतिशीलता और सामाजिक नीतियों में अंतर को दर्शाती है।
-
विकसित देश : विकसित देशों में, युवा बेरोज़गारी दर अक्सर समग्र बेरोज़गारी दर से अधिक होती है, जो युवाओं को श्रम बाज़ार में प्रवेश करने में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से युवा बेरोज़गारी दर लगातार उच्च बनी हुई है, स्पेन और ग्रीस जैसे देशों में यह दर 30% से अधिक है।
-
विकासशील देश : विकासशील देशों में, युवा बेरोज़गारी की विशेषता अक्सर अल्परोज़गार, अनौपचारिक रोज़गार और अनिश्चित कार्य स्थितियों से होती है। हालाँकि इन क्षेत्रों में समग्र बेरोज़गारी दर कम हो सकती है, लेकिन कई युवा कम वेतन वाली, असुरक्षित नौकरियों में काम करते हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा या श्रम अधिकारों तक पहुँच नहीं होती।
-
उभरती अर्थव्यवस्थाएँ : उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, युवा बेरोज़गारी अक्सर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी अपनाने जैसे तेज़ आर्थिक बदलावों से प्रेरित होती है। जबकि ये बदलाव नए रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे नौकरी के विस्थापन और कौशल बेमेल का कारण भी बन सकते हैं, खासकर युवा लोगों के लिए।
कोविड-19 का प्रभाव: कोविड-19 महामारी ने युवाओं के रोज़गार पर गहरा असर डाला है, जिससे मौजूदा चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं और नई चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। युवा लोग नौकरी छूटने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ख़ास तौर पर खुदरा, आतिथ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में, जो महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। दूर से काम करने की ओर बदलाव और डिजिटलीकरण की गति ने भी युवाओं के लिए नई बाधाएँ खड़ी कर दी हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास तकनीक या डिजिटल कौशल तक पहुँच नहीं है।
ILO का अनुमान है कि महामारी ने "लॉकडाउन पीढ़ी" को जन्म दिया है, जिसमें लाखों युवा लंबे समय तक बेरोज़गारी, काम के घंटे कम होने और श्रम बाज़ार में प्रवेश में देरी का सामना कर रहे हैं। इस संकट का असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जा सकता है, क्योंकि युवा लोगों को शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्य अनुभव खोने के दीर्घकालिक परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।
युवा बेरोजगारी के कारण
युवा बेरोज़गारी एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए कई कारक ज़िम्मेदार हैं। युवा रोज़गार संकट से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के लिए इन कारणों को समझना ज़रूरी है।
शिक्षा और कौशल में बेमेल : युवा बेरोज़गारी के प्राथमिक कारणों में से एक युवाओं के पास मौजूद कौशल और नियोक्ताओं की ज़रूरतों के बीच बेमेल है। कई देशों में, शिक्षा प्रणाली श्रम बाज़ार की माँगों के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित नहीं है, जिसके कारण युवाओं द्वारा स्कूल में हासिल किए गए कौशल और उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल के बीच अंतर पैदा होता है।
-
प्रासंगिक कौशल की कमी : कई युवा लोग उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता के बिना श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सच है, जिनमें विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा।
-
अति योग्यता : कुछ मामलों में, युवा लोग अपने लिए उपलब्ध नौकरियों के लिए अति योग्य हो सकते हैं, जिससे अल्प-रोज़गार की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब युवा लोग अपनी योग्यता से मेल खाने वाली नौकरी पाने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कम-कुशल या कम-भुगतान वाली नौकरियाँ स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
-
अपर्याप्त कैरियर मार्गदर्शन : स्कूलों में कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श की कमी कौशल बेमेल में योगदान दे सकती है, क्योंकि युवा लोग ऐसे शैक्षिक पथ चुन सकते हैं जो श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में स्नातकों की अधिकता हो सकती है और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो सकती है।
आर्थिक और श्रम बाजार की स्थितियां: आर्थिक स्थितियां और श्रम बाजार की गतिशीलता युवाओं के रोजगार परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक मंदी के दौर में, युवा लोग अक्सर सबसे पहले अपनी नौकरी खो देते हैं और सबसे आखिर में उन्हें ही काम पर रखा जाता है, क्योंकि नियोक्ता अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने को प्राथमिकता देते हैं।
-
आर्थिक मंदी : आर्थिक मंदी और मंदी के कारण नौकरी के अवसरों में कमी आ सकती है, खासकर उन युवाओं के लिए जो श्रम बाजार में नए हैं। उदाहरण के लिए, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, कई देशों में युवा बेरोजगारी दर में उछाल आया, जिससे प्रभावित पीढ़ी पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।
-
श्रम बाजार में लचीलापन : श्रम बाजार में लचीलापन, समग्र रोजगार स्तरों के लिए फायदेमंद होते हुए भी, युवा लोगों के लिए नौकरी की असुरक्षा और अनिश्चित कार्य को भी बढ़ा सकता है। कुछ देशों में, लचीलेपन को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए श्रम बाजार सुधारों के परिणामस्वरूप अस्थायी, अंशकालिक और अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से युवा श्रमिकों के बीच।
-
वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन : वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन ने श्रम बाज़ारों को बदल दिया है, नए अवसर पैदा किए हैं और साथ ही पारंपरिक नौकरियाँ भी खत्म की हैं। युवा लोग, खास तौर पर वे लोग जिनके पास नए और उभरते उद्योगों के लिए ज़रूरी कौशल नहीं हैं, अक्सर इन परिवर्तनों से असंगत रूप से प्रभावित होते हैं।
सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक: लिंग, नस्ल, जातीयता और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक भी युवाओं के रोज़गार परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। कई मामलों में, ये कारक आर्थिक और श्रम बाज़ार की स्थितियों के साथ मिलकर युवाओं के लिए अतिरिक्त बाधाएँ पैदा करते हैं।
-
लैंगिक असमानता : लैंगिक असमानता युवाओं के रोजगार में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है, खासकर युवा महिलाओं के लिए। कई देशों में, युवा महिलाओं को युवा पुरुषों की तुलना में अधिक बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ता है, साथ ही कुछ उद्योगों या व्यवसायों में प्रवेश करने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भेदभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता और कार्य-जीवन संतुलन के लिए समर्थन की कमी इन असमानताओं में योगदान करती है।
-
नस्लीय और जातीय असमानताएँ : युवा रोजगार में नस्लीय और जातीय असमानताएँ कई देशों में प्रचलित हैं, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दर्शाती हैं। अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के युवा अक्सर उच्च बेरोज़गारी दर, कम वेतन और शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुँचने में अधिक बाधाओं का सामना करते हैं।
-
सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि : सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि युवाओं के रोज़गार परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम आय वाले परिवारों के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोज़गार में बाधाओं का सामना करने की अधिक संभावना होती है, जिससे बेरोज़गारी दर अधिक होती है और ऊपर की ओर बढ़ने के अवसर सीमित होते हैं।
संस्थागत और नीतिगत कारक: श्रम बाजार संस्थानों, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता जैसे संस्थागत और नीतिगत कारक भी युवा रोजगार परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
-
श्रम बाजार संस्थाएँ : ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और सामूहिक सौदेबाजी तंत्रों जैसी मज़बूत श्रम बाजार संस्थाएँ युवा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उचित वेतन और कार्य स्थितियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। कमज़ोर श्रम बाजार संस्थाओं वाले देशों में, युवा लोगों को अनिश्चित रोज़गार और शोषण का सामना करने की अधिक संभावना होती है।
-
सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ : बेरोज़गारी लाभ, सामाजिक बीमा और आय सहायता कार्यक्रमों सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ युवा लोगों पर बेरोज़गारी के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीमित या अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों वाले देशों में, युवा लोग गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
-
सरकारी नीतियाँ : सक्रिय श्रम बाज़ार कार्यक्रम, युवा रोज़गार पहल और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सरकारी नीतियाँ युवा रोज़गार परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। प्रभावी नीतियाँ युवाओं को शिक्षा से रोज़गार की ओर बढ़ने में मदद कर सकती हैं, जबकि अप्रभावी या खराब तरीके से लक्षित नीतियाँ युवा बेरोज़गारी को बढ़ा सकती हैं।
युवा बेरोजगारी के परिणाम
युवा बेरोज़गारी के व्यक्तियों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर दूरगामी परिणाम होते हैं। इन परिणामों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों सहित विभिन्न आयामों में देखा जा सकता है।
सामाजिक परिणाम: युवा बेरोजगारी के गंभीर सामाजिक परिणाम होते हैं, जो युवाओं के कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक एकीकरण को प्रभावित करते हैं।
-
मानसिक स्वास्थ्य : बेरोज़गारी का युवा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे निराशा, चिंता और अवसाद की भावनाएँ पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक बेरोज़गारी के कारण आत्म-सम्मान और पहचान की भावना में कमी आ सकती है, साथ ही मादक द्रव्यों के सेवन और सामाजिक अलगाव का जोखिम भी बढ़ सकता है।
-
सामाजिक बहिष्कार : बेरोज़गारी सामाजिक बहिष्कार का कारण बन सकती है, क्योंकि युवा लोग सामाजिक नेटवर्क, सामुदायिक गतिविधियों और नागरिक भागीदारी से कट सकते हैं। इससे अलगाव और हाशिए पर होने की भावना पैदा हो सकती है, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए।
-
विलंबित जीवन परिवर्तन : युवा बेरोज़गारी जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों में देरी कर सकती है, जैसे घर छोड़ना, परिवार बनाना और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसका युवाओं के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
आर्थिक परिणाम: युवा बेरोजगारी के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होते हैं, जो व्यक्तियों और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं।
-
खोई हुई आय और आर्थिक असुरक्षा : बेरोज़गारी के कारण युवा लोगों की आय कम हो जाती है, जिससे आर्थिक असुरक्षा और गरीबी बढ़ती है। इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जो युवा अपने करियर की शुरुआत में बेरोज़गारी का अनुभव करते हैं, उन्हें भविष्य में कम वेतन और नौकरी की अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।
-
मानव पूंजी का कम उपयोग : युवा बेरोजगारी मानव पूंजी के महत्वपूर्ण कम उपयोग को दर्शाती है, क्योंकि युवा लोग जो काम पाने में असमर्थ हैं, वे आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान करने में असमर्थ हैं। इससे संभावित उत्पादकता और नवाचार का नुकसान हो सकता है।
-
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि : युवा बेरोज़गारी के उच्च स्तर के कारण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, जैसे कि बेरोज़गारी लाभ, सामाजिक सहायता और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो सकती है। इससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ सकता है और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं।
राजनीतिक परिणाम: युवा बेरोजगारी के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और संस्थाओं में विश्वास की कमी हो सकती है।
-
सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता : युवा बेरोज़गारी के उच्च स्तर सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि आर्थिक अवसरों से वंचित महसूस करने वाले युवा राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग हो सकते हैं। इसका परिणाम विरोध, प्रदर्शन और यहां तक कि हिंसा भी हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां असमानता और सामाजिक तनाव का स्तर बहुत अधिक है।
-
संस्थाओं में विश्वास की कमी : युवा बेरोज़गारी के कारण सरकार, राजनीतिक दलों और श्रम बाज़ार संस्थाओं सहित संस्थाओं में विश्वास की कमी हो सकती है। जिन युवाओं को लगता है कि नीति निर्माताओं द्वारा उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वे राजनीतिक प्रक्रिया से विमुख हो सकते हैं, जिससे नागरिक भागीदारी और मतदाता मतदान में गिरावट आ सकती है।
युवा बेरोजगारी की समस्या का समाधान: संभावित समाधान
युवा बेरोज़गारी को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज संगठनों सहित कई हितधारक शामिल हों। युवा रोज़गार को बढ़ावा देने और बेरोज़गारी को कम करने के लिए कई प्रमुख रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं।
शिक्षा और कौशल विकास
-
शिक्षा को श्रम बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ना : शिक्षा प्रणालियों को श्रम बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युवा नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कौशल और योग्यताएं हासिल कर सकें। इसमें पाठ्यक्रम को अपडेट करना, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना और शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
-
आजीवन सीखने में निवेश करना : युवाओं को श्रम बाजार की बदलती मांगों के अनुकूल ढलने में मदद करने के लिए आजीवन सीखना और कौशल विकास आवश्यक है। सरकारों और नियोक्ताओं को युवाओं को नए कौशल हासिल करने और श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसरों में निवेश करना चाहिए।
-
करियर मार्गदर्शन और परामर्श में सुधार : प्रभावी करियर मार्गदर्शन और परामर्श युवाओं को उनकी शिक्षा और करियर पथ के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छात्रों को श्रम बाजार के रुझान, नौकरी के अवसरों और विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
आर्थिक और श्रम बाज़ार नीतियां
-
युवा रोजगार पहल को बढ़ावा देना : सरकारों को लक्षित युवा रोजगार पहलों को लागू करना चाहिए, जैसे कि वेतन सब्सिडी, प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप, ताकि युवाओं को शिक्षा से रोजगार में संक्रमण में मदद मिल सके। ये कार्यक्रम युवाओं को मूल्यवान कार्य अनुभव प्रदान कर सकते हैं और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार कर सकते हैं।
-
श्रम बाजार विनियमन को मजबूत करना : श्रम बाजार विनियमन को युवा श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, साथ ही लचीलेपन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करना, उचित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करना और सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
-
उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करना : उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सरकारों और वित्तीय संस्थानों को युवा उद्यमियों को वित्तपोषण, मार्गदर्शन और व्यवसाय विकास सहायता तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद मिल सके।
सामाजिक संरक्षण और समावेशन
-
सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का विस्तार : बेरोज़गारी या अनिश्चित काम का सामना कर रहे युवाओं के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें बेरोज़गारी लाभ, आय सहायता और स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच शामिल हो सकती है।
-
सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देना : श्रम बाजार में सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए, खास तौर पर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए। इसमें भेदभाव विरोधी नीतियों को लागू करना, भर्ती में विविधता को बढ़ावा देना और समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करना शामिल हो सकता है।
-
लैंगिक असमानता को संबोधित करना : लैंगिक असमानता को संबोधित करना युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर युवा महिलाओं के लिए। सरकारों और नियोक्ताओं को कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए, जैसे समान वेतन, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, और कार्य-जीवन संतुलन के लिए समर्थन।
वैश्विक सहयोग और एकजुटता
-
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना : वैश्विक युवा रोज़गार संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नीतिगत प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने और युवा बेरोज़गारी के उच्च स्तर का सामना करने वाले देशों को सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
-
विकासशील देशों को सहायता देना : विकासशील देशों को युवा बेरोज़गारी को संबोधित करने में अक्सर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित संसाधन, कमज़ोर संस्थान और अनौपचारिकता का उच्च स्तर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकास सहायता, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के माध्यम से इन देशों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।
-
वैश्विक युवा नेटवर्क को बढ़ावा देना : वैश्विक युवा नेटवर्क युवा रोजगार को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये नेटवर्क युवाओं को आपस में जुड़ने, अनुभव साझा करने और ऐसी नीतियों की वकालत करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं जो सभी के लिए अच्छे काम और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देती हैं।
निष्कर्ष: युवा बेरोज़गारी एक वैश्विक चुनौती है जिसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हैं। इस संकट से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज संगठनों सहित कई हितधारक शामिल हों। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके, युवा रोज़गार पहलों को बढ़ावा देकर, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करके और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर, हम दुनिया भर के युवाओं के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। युवा बेरोज़गारी को कम करने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन व्यक्तियों, समाजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावित लाभ बहुत ज़्यादा हैं। एक साथ काम करके, हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहाँ सभी युवाओं को सम्मान, सुरक्षा और अवसर का जीवन जीने का अवसर मिले।
What's Your Reaction?